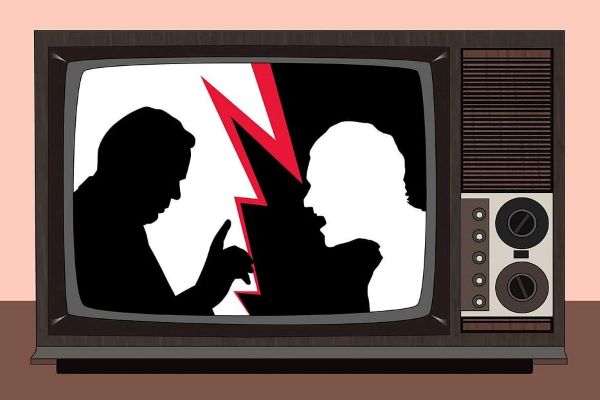अजय बोकिल
ओपीनियन पोल, एग्जिट पोल, काउंटिंग ट्रेंड और एक्जेक्ट रिजल्ट। हर चुनाव की वो स्टेप्स हैं, जिनको नापना चुनाव विश्लेषक की जिम्मेदारी और शगल होता है। हकीकत में उन्हें उड़ती चिडि़या को देखकर बताना होता है कि वो किस डाल पर बैठेगी। अब चिडि़या है कि कई बार उस डाल पर जा बैठती है, जो विश्लेषकों की नापसंद होती है या कई दफा वो किसी भी डाल पर बैठने के बजाए फुर्र से उड़ जाती है या फिर आसमान में ही पर मारती रहती है। चुनाव विश्लेषक चिडि़या की हर अदा का विश्लेषण इस अंदाज में करते हैं कि मानो चिडि़या उन्हीं से पूछकर उड़ी थी।
वैसे कई चुनाव विश्लेषक अपनी राय जताते हुए यह भी कहे जाते हैं कि वो जो कह रहे हैं, अंतिम परिणाम वैसा होगा, जरूरी नहीं है। टीवी चैनल से चिपका दर्शक समझ नहीं पाता कि इस जुमले का निश्चित अर्थ क्या है। दरअसल चुनाव नतीजों को समझना जितना आसान है, चलती मतगणना में उसके सटीक विश्लेषण का काम बहुत कठिन और जोखिम भरा होता है।
यूं चुनाव विश्लेषण पहले भी होते थे, लेकिन उसमें जनमत के रुझान या सतह के नीचे खदबदा रहे असंतोष को भांपने की कोशिश ज्यादा होती थी। चुनाव नतीजे क्या होंगे, क्या होने चाहिए, ऐसी भविष्यवाणी करने के बजाए नतीजों के कारणों और प्रवृत्तियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुआ करता था। लेकिन टीवी का जमाना आने के बाद ‘चुनावी ज्योतिषगिरी’ इतनी हावी हो गई है कि इस चक्रव्यूह में ज्यादातर दर्शक ही बेवकूफ बनता है। उस पर सोशल मीडिया भी आ जाने के बाद तो फौरी बौद्धिक विश्लेषणों में से ‘धैर्य’ शब्द डिलीट ही हो गया है। यानी पत्ता खड़कने को भी आंधी बता दिया जाता है और अंडर करंट हो तो पास के चश्मे से भी साफ नहीं दिखता। यही नहीं बिना किसी अफसोस के मूर्खता करते जाने का ट्रेंड भी सोशल मीडिया ने ही सेट किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगता है फिर एक बार चुनाव विश्लेषकों की पुंगी बजाने वाले रहे। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था। राज्य में शुरुआती रुझानों के आधार पर बिहार में भगवा सरकार बनने का स्वस्ति वाचन विश्लेषकों/चैनलों ने शुरू कर दिया था, लेकिन घंटे भर में ही तस्वीर पूरी तरह उलट गई। लालू-नीतीश का गुणगान होने लगा। चुनाव विश्लेषक भी हक्के-बक्के रह गए। काटो तो खून नहीं वाली स्थिति।
इस बार फिर बिहार ने चुनाव विश्लेषकों को गच्चा दे दिया है। एग्जिट पोल से चढ़े अरमानों पर एक्जेक्ट पोल ने ठंडा पानी डाल दिया। यानी सुबह धूप तेज होने तक युवा तेजस्वी के राजनीतिक तेज का महिमागान करने वाले सूरज ढलते महागठबंधन की गलतियां हमें बताने लगे। फिर मामला ट्वेंटी-ट्वेंटी के रोमांच पर अटक गया। आखिरी बाजी राजग के हाथ रही। उधर स्टूडियो में बैठे चुनाव विश्लेषक यह गले उतारने मे जुट गए कि नीतीश अभी भी जमीनी नेता हैं और भाजपा की रणनीतिक खूबियां क्या रहीं? या फिर महागठबंधन किस ताकत से टक्कर दे रहा है।
दरअसल फौरी और कुछ हद तक अंधेरे में किए जाने वाले चुनाव विश्लेषण का यह काम शादी में बरातियों को झेलने जितना नाजुक और कठिन है। कब कौन बिदक जाए, क्या पता। एक जमाने में ओपिनियन पोल का भी विश्लेषण हुआ करता था। लेकिन सबसे अजीब और तलवार की धार पर चलने जैसा विश्लेषण ‘एक्जिट पोल’ का होता है। दूसरे की टोकरी में अंडे रखने जैसा। सारे आंकड़े उस एजेंसी के जुटाए होते हैं, जो किसी टीवी चैनल के साथ गठबंधन में अपना सर्वेक्षण करती है।
यह एजेंसी किन, कितने लोगों से और कब, क्या जानकारी बटोरती है, पता नहीं। लेकिन टीवी एंकर ऐसे सर्वेक्षणों की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता पर लंबे-चौड़े प्रवचन देते जरूर दिखते हैं। अपना अनुभव रहा कि सालों पहले एक आम चुनाव के जनमत सर्वे की मप्र की रिपोर्ट एक सर्वेयर मेरे पास दो घंटे बैठकर ही ले गया था। जाते समय बोला, सर मेरा काम हो गया। चुनाव नतीजों के पहले यह सेम्पल सर्वे ही होता है, जो कुल वोटरों के 0.001 फीसदी से भी कम लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर होता है।
वोटर जो जानकारी सर्वे एजेंसी को देता है, वह कितनी सच होती है, कहना मुश्किल है। ज्यादातर मामलों में तो पति-पत्नी को आपस में भी पता नहीं होता कि कौन किस पार्टी का बटन दबाकर आया है। अलबत्ता चुनाव विश्लेषक अपने सहज और सामान्य ज्ञान के आधार पर कुछ न कुछ विश्लेषण करते रहते हैं। इस भरोसे के साथ कि तुक्का कभी भी तीर बन सकता है। साथ में यह भी ध्यान रखना होता है कि सम्बन्धित टीवी चैनल की टीआरपी में बरकत हो। यही वजह है कि जो विश्लेषक सुबह तक जिस पार्टी के जीतने का गहन विश्लेषण करता दिखता है, शाम को उसी पार्टी की नाकामियों के कारणों पर विस्तार से रोशनी डालने से नहीं चूकता। हकीकत में चुनाव नतीजे क्या होंगे, यह विश्लेषक तो क्या गिनती से पहले भगवान को भी पता नहीं होता।
टीवी चैनलों की मजबूरी यह है कि उन्हें चुनाव परिणामों को एक ‘सीरियल थ्रिलर’ की तरह दिखाना ही है। क्योंकि मतदाता की जिज्ञासा दोहन का यह सबसे कारगर तरीका है और चैनल की कमाई का भी। लिहाजा कुछ विश्लेषक तो दिन भर के लिए बुक होते हैं तो कुछ तात्कालिक तौर पर ऑनलाइन जोड़े जाते हैं। चुनाव विश्लेषकों की एक नस्ल ऐसी भी है, जो अंतिम नतीजे आने तक स्टूडियो में ही कुंडली मारकर बैठती है। बहुत से टीवी चुनाव विश्लेषक चैनल के राजनीतिक रुझान के माफिक नतीजों की व्याख्या करते चलते हैं। कभी-कभार इस विश्लेषण में उबाल लाने के लिए दो विश्लेषकों को भिड़ा भी दिया जाता है। ताकि दर्शक चैनल चेंज करना भूल जाए।
वैसे ये चुनाव विश्लेषक भी कई तरह के होते हैं। पहले तो उन राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, जो एक तयशुदा शब्दावली में अपनी पार्टी की हर मूर्खता का बचाव और प्रतिद्वंद्वी पार्टी की हर बात को खारिज करने काम करते रहते हैं। शायद प्रतिस्पर्द्धी पार्टी की निकृष्टतम आलोचना से ही प्रवक्ता विश्लेषकों के तमगे तय होते हैं। ऐेसे में ये क्या कहने वाले हैं, यह एंकर को, स्टूडियों में बैठे पैनलिस्ट को और बाहर सिर पकड़ कर बैठे दर्शक को पहले से पता होता है।
कुछ विश्लेषक सामयिक या अचानक एंट्री वाले होते है। इनकी उपलब्धता ही इनकी योग्यता होती है। इन्हें सम्बन्धित चैनल पर चुनाव नतीजों के बारे में पहले क्या दिखाया या बताया गया है, इसकी जानकारी नहीं के बराबर होती है। फिर भी वे एंकरों के बेतुके सवालों का सटीक जवाब देते हैं और खुद भी कुछ सवाल छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
एक और श्रेणी ‘बंधुआ मजदूर’ टाइप चुनाव विश्लेषकों की होती है। इन्हें बुलाया तो तय समयावधि के लिए जाता है, लेकिन एक बार स्टूडियो के पैनलिस्ट में शामिल होने के बाद वो खूंटे से बंध जाते हैं। उन्हें चाय पर चाय पिलाई जाती है। वो तब तक चुनाव विश्लेषण करते रहते हैं, जब तक उनका कोई रिलीवर नहीं आ जाता। कई बार तो चुनाव विश्लेषण के सारे तर्क खत्म होने और एंकर के एक ही सवाल का अलग-अलग तरीके से जवाब दे चुकने के बाद भी विश्लेषण उनका पीछा नहीं छोड़ता।
उधर एंकर बार-बार यही कहे जाते हैं कि देखते रहिए फलां-फलां चैनल। इधर दर्शक सिर पीटने लगता है, क्योंकि जो ‘खुला रहस्य’ है, उसे सस्पेंस बनाए रखने में टीवी वाले पूरी ताकत झोंके रहते हैं। चुनाव विश्लेषकों की एक और श्रेणी ‘अजेंडा विश्लेषकों’ की होती हैं। नतीजे उनकी सोच या वैचारिक आग्रह के अनुरूप हैं या नहीं, इस बात को वो पूरी दमदारी से समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए जरूरी नहीं होता कि उन्हें जमीनी हकीकत का भी ठीक से पता हो।
कुछ चुनाव विश्लेषक जरूर पूरी संजीदगी के साथ नतीजों का हर पहलू दर्शकों को बताते हैं। ऐसे वस्तुनिष्ठ विश्लेषक अमूमन संख्या में अल्प होते हैं और उन्हें गंभीर विश्लेषण के लिए बुलाया भी जाए, यह जरूरी नहीं होता। बहुतायत उन पलटीमार विश्लेषकों की होती है, जो रुझानों के हिसाब से विश्लेषण का भी रंग बदलते चलते हैं। कई बार तो ये विश्लेषक चुनाव परिणामों से पहले ही दर्शकों के गले यह उतारने की कोशिश करते हैं कि जो वो सोचते हैं, जनता भी वही सोच रही है या फिर जनता को वैसा ही सोचना चाहिए। वह नहीं सोच रही तो यह जनता की गलती है।
यहीं सारा गड़बड़झाला है। क्योंकि ऐसे में जनता की सोच और विश्लेषक की सोच में कई बार गजब की ‘डिस्टेंसिंग’ दिखाई पड़ती है। बाज दफा उन्हें ‘जनता की इच्छा सर्वोपरि’ का मास्क भी लगाना पड़ता है। यानी चाहत कुछ होती है, नतीजा कुछ आता है। उधर टीवी चैनल वाले बाग-बाग रहते हैं कि उनका ‘काम’ हो गया।